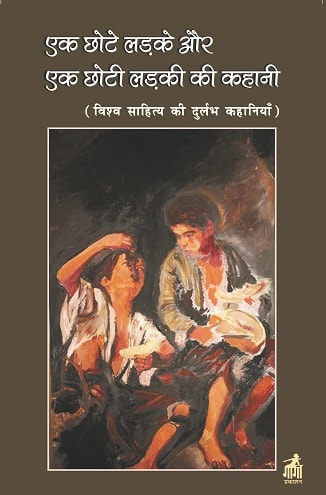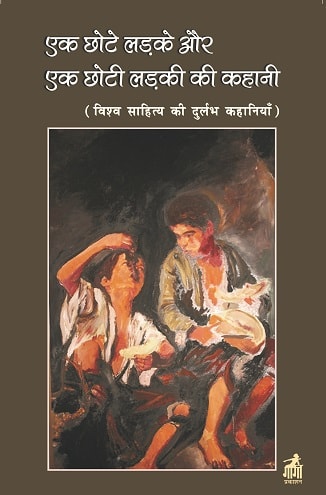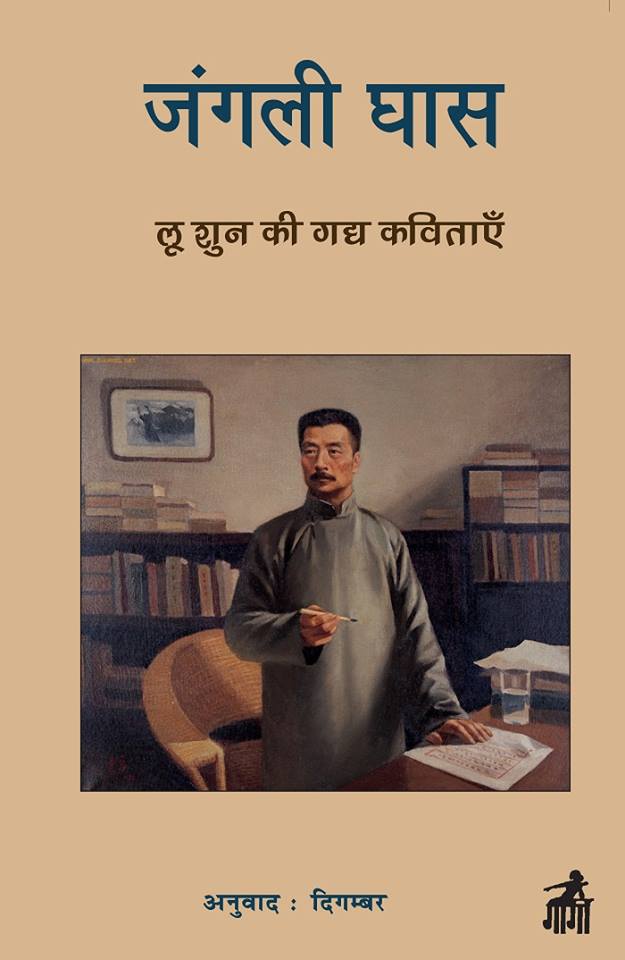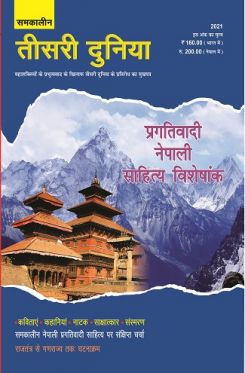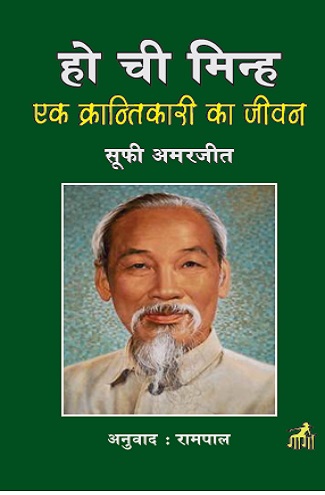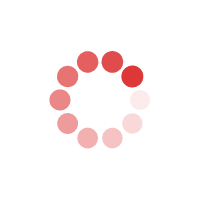कृषि संकट को समझने के लिए – दो जरूरी किताबें
द्वारा In Book Review agrarian crisisप्रवीन कुमार
भारत के किसान लम्बे समय से एक भयावह और जानलेवा कृषि संकट की गिरफ्त में है। बड़े फार्मर और धनी किसान भले ही इस संकट से ज्यादा प्रभावित न हुए हों, लेकिन देश के कुल किसानों का 90 प्रतिशत- छोटे और मध्यम किसान इस संकट के कारण लाखों की संख्या में आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। सरकारों के कई नीम-हकीमी उपायों के बावजूद भी यह संकट लगातार बढ़ता गया है। छोटी जोत की आय से किसान परिवार का गुजारा चलना मुश्किल हो गया है। ये किसान परिवार कर्ज समेत अनेकों समस्याओं के भारी बोझ तले दबे हैं।
तात्कालिक और स्थानीय मांगों को लेकर किसानों के आन्दोलन और सरकारों द्वारा उनका लाठी-गोली से दमन रोजमर्रे की बात बन चुकी है। मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों ने किसानों और उनकी समस्याओं से पल्ला झाड़ लिया है। संसदीय राजनीति में खेती-किसानी पर गंभीर चर्चा करना इतिहास की बात हो गयी है।
इस निराशा भरे माहौल में भी देश-दुनिया के कुछ जनपक्षधर बुद्धिजीवियों ने आज के खेती के संकट को समझने का प्रयास किया है, और लगातार कर रहे हैं।
दुनियाभर में मशहूर पत्रिका ‘मन्थली रिव्यू’ में इस विषय पर बहुत से लेख आये हैं। जिनमें से कुछ खास लेखों को चुनकर उनका हिंदी में अनुवाद करके ‘गार्गी प्रकाशन’ ने  ’ के नाम से छापा है।
’ के नाम से छापा है।
भारत समेत पूरी दुनिया में खेती के मौजूदा संकट को समझने के लिए इन दोनों पुस्तकों के लेख ठोस सैद्धान्तिक आधारप्रदान करते हैं। ये लेख खेती में पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली की घुसपैठ और खेती पर उसके कब्जे, मौजूदा संकट के वैश्विक स्वरुप और उसके असमाधेय हो जाने तथा पिछली सदी में इस संकट के चीन द्वारा पेश किये गये समाधान की वैज्ञानिक जांच-पड़ताल करते हैं।
इन पुस्तकों की भाषा सैद्धान्तिक और गूढ़ तो जरुर है लेकिन खेती-किसानी का कोई संकट इसके दायरे से बाहर नहीं हैं। अगर हम अखरोट फोड़ कर उसकी गिरी का मजा लेने की हिम्मत करें तो ये पुस्तकें हमें खेती के तमाम संकटों, उनके कारणों और उनके समाधान को बहुत गहराई से समझा देती हैं। यहां हम इन पुस्तकों के कुछ जरूरी मुद्दों को संक्षेप में दे रहे हैं, ताकि पाठकों को इसका अंदाजा लगे कि कृषि और खाद्य संकट की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसका जिम्मेदार कौन है।
खेती का संकट देवी सीता की तरह किसी घड़े से अचानक प्रकट नहीं हुआ हैं। इसकी जड़ें खेती के विकास के लिए शासक वर्गों की नीतियों और यूरोप की औद्योगिक क्रांति द्वारा खेती पर थोपे गये उद्योग के वर्चस्व में हैं। यह खेतीहर पैदावार के लिए अपनायी गयी उस पूूंजीवादी प्रणाली के विकास का लाजिमी नतीजा है जिसका मकसद आदमी की बुनियादी जरूरतें पूरी करना नहीं बल्कि मुनाफा लूटना है।
अपने शुरुआती दौर में पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली ने ईश्वर और उसके पुत्रों–राजे-रजवाड़ों की सत्ता को ढहाकर अपनी शानदार भूमिका निभायी थी और सत्ता के केंद्र में ईश्वर के बजाय मानव को स्थापित किया था। लेकिन पुरानी दुनिया के खंडहरों पर जो नयी दुनिया बनाई गयी, वह बाज़ार और मुनाफे पर टिकी थी।
पूंजी को लगातार बढ़ाते जाना, वरना अपनी मौत को दावत देना पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का अंतिम मकसद होता है। लेकिन खेती में पूंजी की घुसपैठ धीरे-धीरे और लम्बी प्रक्रिया में होती है जो उद्योगों में उत्पादन के उस तौर तरीके से भिन्न रूप में होती हैं, जिसे अट्ठारवीं और उन्नीसवीं सदी के कपड़ा बुनने के उदाहरण से समझा जाता है।
इस अंतर का कारण खेती के मूल चरित्र में है। खेती से पैदावार करने में जमीन ही सबसे बुनियादी साधन है। उद्योग में तकनीक का विकास करके मशीनरी आदि साधनों की लागत को लगातार घटाया जा सकता है लेकिन जमीन के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। साथ ही उद्योग की लागतों की तरह इसकी बड़े पैमाने पर और नकदी में खरीद-बिक्री आसान नहीं है। उद्योग में बहुत से मजदूर एक छोटी जगह में मालिकों या मैनेजरों की नजरों के सामने काम करते हैं। जबकि दूर तक फैले बड़े-बड़े फार्मों में सब मजदूरों पर एकसाथ निगाह नहीं रखी जा सकती। मौसम में होने वाले उतार-चढाव का उद्योग पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता लेकिन खेती में पाला, गर्मी, ज्यादा बरसात, आंधी-तूफान एक-दो दिन में ही पूरी फसल को चौपट कर सकते हैं। खेती में कीट-पतंगे, बीमारियां तैयार फसल को तबाह कर देती हैं लेकिन उद्योग में ऐसा कोई डर नहीं है। खेती में कभी तो मजदूरों के लिए कोई काम नहीं होता और कभी अचानक बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत हो जाती हैं। जबकि उद्योग में पहले से पता होता है कि कब कितने आदमियों की जरूरत होगी। उद्योग में नयी तकनीक विकसित करके उत्पादन की रफ्तार बढ़ायी जा सकती है लेकिन खेती में हर फसल के पकने का समय तय है, उसे घटाया नहीं जा सकता। इन्हीं कारणों के चलते खेती में पूूंजी की घुसपैठ धीरे-धीरे और उद्योग से अलग तरीकों से होती है।

राजे-रजवाड़ों के पुराने सामंती जमाने में किसान अपने परिवार और खेती की जरूरतों की पूर्ति या तो खुद ही कर लेता था या फिर बढई, लोहार, जुलाहे आदि पेशों में लगे लोगों का श्रम फसलाने के हिसाब से खरीदकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करता था। बीज, खाद, हल बैल, खेती के साधारण औजार जैसी खेती की तमाम लागतें और आड़े वक्त के लिए श्रम या तो उसका अपना होता या फिर वह फसलाने और डंगवारे जैसे तरीकों से गांव से ही जुटा लेता था। इसी तरीके से रोटी कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी इंसानी जरूरतें भी पूरी हो जाती थी। गांव के कारीगर को पता होता था कि वह अमुक चीज किसके लिए बना रहा है और क्यों बना रहा है। इसी तरह किसान को भी पता होता था कि उसने फसल का कौन सा हिस्सा किसके लिए उगाया है। खेती की लागतें और पैदावार दोनों उसकी अपनी थी। खेती किसान की आमदनी का नहीं, बल्कि उसकी जरूरतों को पूरा करने का साधन थी।
किसान अपनी जरूरत को ध्यान में रखकर ही फसल उगाता था। फसल की लगभग सारी उपज किसान के परिवार, खेती की जरूरतों और सामंती लगान और नजरानों पर ही खर्च हो जाती थी। बाज़ार में किसान कभी-कभार ही अपनी उपज का कोई मामूली हिस्सा बेचता था। किसान की बचत को सामंती प्रभु लगान और उसके साथ-साथ किसान पर तरह तरह के जुर्माने, नजराने थोपकर जबरन हथिया लेते थे। इसके अलावा धर्म के ठेकेदार कभी जजिया कर लगाकर कभी दशमांश लगाकर किसान को लूटते थे। कुल मिलाकर सारे किलों, महलों, मंदिरों, मस्जिदों का बोझ किसान की पीठ पर ही लदा था। नतीजन किसान के समृद्ध होने की कोई गुंजाईश नहीं थी।
दुनिया अपनी गति से बदलती भी जा रही थी। पैदावार भी बढ़ रही थी, व्यापार भी बढ़ रहा था, दस्तकारी और खेती के औजारों में बदलाव आ रहे थे, लेकिन उनकी रफ़्तार बहुत धीमी थी। इसी दौरान यूरोप में एक नयी दुनिया गढ़ी जा रही थी वहां से उठे तूफ़ान ने दुनिया के बदलाव की रफ़्तार बहुत तेज़ कर दी। वहां नया विज्ञान, समाज और नयी-नयी संस्थाएं पैदा हुई। नये-नये औजार और नयी-नयी मशीनें बनने लगी। उत्पादन करने के लिए कारखाने लगे जिससे उत्पादन की रफ़्तार बहुत तेज़ हो गयी। इस माल को तैयार करने के लिए कच्चे माल और बेचने के लिए बाज़ार की तलाश में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचने के लिए नये-नये रस्ते खोजे गये। दुनिया में व्यापार बहुत तेज़ हो गया। इसी व्यापार के जरिये दुनिया के अधिकांश हिस्से पर यूरोपियों ने कब्ज़ा किया। हमारे देश को भी अंग्रेजो ने गुलाम बनाया।
यह नया ज़माना खेती में भी नये बदलाव लेकर आया। भूपतियों को नयी-नयी चीजें खरीदने के लिए ज्यादा नकदी की जरूरत पड़ी। दुनिया में इतने ज्यादा किस्म के माल तैयार हो रहे थे कि बिना नकदी के कुछ भी लेन-देन या व्यापार संभव ही नहीं था। किसान पर भी नकद लगान के लिए दबाव पड़ा तो उसने फसल बेचने के लिए बाज़ार का रुख किया। बाज़ार के साथ रिश्ता बनते ही खेती और किसान की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आया। जैसे-जैसे दुनिया में नये-नये माल आते गये, भूपति किसान पर लगन का बोझ बढ़ाते गये। इसके अलावा भी बहुत सी तब्दीलियों ने किसान की नकदी की जरूरत को बढ़ाया। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने और ज्यादा नकदी हासिल करने का दबाव बढ़ता ही गया।
जमीन को रबर की तरह नहीं बढाया जा सकता था। किसान के सामने एक ही रास्ता था कि वह दिये गये रकबे में ही ज्यादा से ज्यादा पैदावार करे। इसके लिए खेती की लागतों में नयी नयी चीजें जुड़ती गयीं जैसे सिंचाई के साधन, उर्वरक, कीटनाशक, ज्यादा उपज देने वाले बीज, मशीनें आदि। ये नयी लागतें किसान खुद तैयार नहीं कर सकता था। इन्हें तैयार करने वाले उद्योगों की एक पूरी कतार खड़ी हो गयी और इसके साथ ही किसान की आत्मनिर्भरता भी $खत्म हो गयी। अब किसान अपनी जरूरत के हिसाब से फसलें नहीं उगा सकता था बल्कि उसे वे फसलें उगानी पड़ती जिनकी बाज़ार में ज्यादा मांग थी ताकि वह अपनी उपज बेचकर ज्यादा नकदी हासिल कर सके।
अब बाज़ार माल की खरीद बिक्री का साधारण स्थान नहीं था बल्कि वह जिंदगी के हर पहलू पर काबिज़ एक नयी ताकत बन गया था। अब समाज पर उसी की सत्ता कायम रह सकती थी जिसकी बाज़ार में सत्ता हो। पूूंजीपति वर्ग की अगुवाई में सारी जनता ने मिलकर राजे-रजवाड़ों की सामंती सत्ता को उखाड़ फेंका और सत्ता की बागडोर पूंजीपति वर्ग के हाथ में आयी। किसान जोर-जबरदस्ती की लूट से तो आजाद हो गया लेकिन उससे भी खतरनाक, बाज़ार की लूट के चंगुल में फंस गया।
बाज़ार के विस्तार ने खेती की लागतों के मामले में तो किसान को दूसरों पर निर्भर बनाया ही है साथ ही साथ उसके और उसकी उपज के ग्राहकों के बीच कई बिचौलियों को भी बैठा दिया है। अब किसान व्यापारियों, कम्पनियों या मिलों को अपनी उपज बेचता है और वे उससे खाने-पीने की चीजें तैयार करके सारी जनता को बेचते हैं।
पुराने जमाने की जरूरत की खेती की जगह आज एक बहुत बड़े कृषि खाद्य तंत्र ने ले ली है। इस तंत्र में खेती के साथ-साथ खेती में लगने वाली लागतों का उत्पादन, उपज की ढुलाई, उपज रखने के बड़े-बड़े एयर-कंडीशंड गोदाम, उपज से खाने-पीने की चीजें तैयार करने वाले उद्योग और उन्हें बेचने वाला खुदरा व्यापार शामिल है। इस पूरे तंत्र के अधिकांश हिस्से पर दुनिया की मुठ्ठी भर दैत्याकार कम्पनियों का कब्ज़ा है।
इस तंत्र में छोटे और मध्यम किसान उत्पादक से ज्यादा ग्राहक हैं। वे खेती की बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बिजली, डीजल, मशीनरी जैसी भारी भरकम लागतों के तो ग्राहक हैं ही साथ ही साथ खेती की उपज से तैयार होने वाले मालों और जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरत की दूसरी चीजों के भी ग्राहक हैं। उनकी जोत की पैदावार उनकी खेती और जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी होती जा रही है। खेती की लागतें तैयार करने वाली कम्पनियां अपने उत्पादों का मनमाना दाम रखती हैं। सरकारें इनके साथ खड़ी हैं। मुठ्ठीभर बीज और कीटनाशकों की छोटी-छोटी शीशियों के दाम हजारों में है, लेकिन इन लागतों के बिना खेती करना असंभव है। किसान जेवर बेचें, पशु बेचें या कर्जा लें, उन्हें ये लागतें खरीदनी ही पड़ती हैं।
दूसरी ओर किसान को अपनी उपज का दाम तय करने का हक नहीं है। कम्पनियों के सामने उसकी हैसियत इतनी कमजोर है कि मौजूदा हालत में कोई ताकत उसे यह हक दिला भी नहीं सकती। सरकारों द्वारा तय किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य एक बेहूदा मजाक बनकर रह गया है। किसान के पास जमा बचत होने की हालत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है और वह बैंको या साहुकारों के कर्जों से खर्च चलाता है। ऐसे में कर्जे चुकाने और नयी फसल बोने के लिए उसे अपनी उपज तुरंत बेचनी पड़ती है। किसान के पास न तो दूर-दराज के बाजारों तक फसल को ढो कर ले जाने के साधन हैं और न ही उसके भंडारण की सुविधा। रोजमर्रा के अनुभव से हम देखते हैं कि जब भी किसान की उपज बाज़ार में आती है तो उसकी कीमतें जमीन पर तो क्या पाताल में चली जाती हैं। ऐसे में किसानों को ज्यादा पैदावार करने का दोषी ठहराया जाता है। जबकि सच्चाई यह है की उसी दौरान देश की आबादी का बड़ा हिस्सा इन उपजों के लिए तरस रहा होता है। उपज की कम कीमत का फायदा उठाकर भंडारण करने वाली कम्पनियां बेहद सस्ते दामों पर इस उपज को हथिया लेती हंै और बाद में मनमाने दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाती हैं। हम रिलायंस, आईटीसी और अडानी जैसे कम्पनी समूहों के ऐसे भीमकाय एयर-कंडीशंड गोदामों को हाईवे के किनारे कहीं भी देख सकते हैं।
किसान की अधिकांश उपजें सीधे इस्तेमाल नहीं की जातीं। ये ब्रेड, बिस्कुट, चीनी, तेल, जेम, जैम जैसे हजारों तरह के उपभोक्ता मालों में कच्चे माल या मूल लागत के रूप में इस्तेमाल होती है। किसान की लागतों पर तो कम्पनियों का कब्ज़ा है और वे ही उनका दाम तय करती हैं। लेकिन इन मालों को तैयार करने वाले उद्योगों में किसानों का कोई दखल नहीं, इन पर भी पूरी तरह कम्पनियों का कब्ज़़ा है। यहां से कम्पनियां जो मुनाफा लूटती हैं वह किसान की कल्पना से भी परे है। किसान से 15 रुपए किलो खऱीदे गये गेहूं को पीसकर आई। टी। सी। जैसी कम्पनियां 31 रुपए किलो आटा बेचती हैं। अगर इसी आटे से ब्रेड या बिस्कुट बनाकर बेचें तो उसकी कीमत 100 रुपए किलो से भी ज्यादा बैठती है। 2 रुपए किलो खऱीदे गये आलू का चिप्स बनाकर लेस जैसी कम्पनियां कई सौ रुपए किलो बेचती हैं। ऐसे उदाहरणों की सूची बेहद लम्बी है।
किसान की चौतरफा लूट होती है। सबसे पहले उसे खेती की लागतों में लूटा जाता है। दूसरे, उपभोक्ता मालों के दाम लगातार बढ़ते जाने से बढ़ी महंगाई के जरिये किसान को लूटा जाता है। तीसरे, उसकी उपज सस्ते से सस्ते दामों पर हड़पी जाती है। चौथे, जब किसान की आय उसकी जीवन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती तो मजबूरन उसे बैंको या साहूकारों से मोटे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। उसकी पहले से ही नाकाफी आय में एक और चोर घुस जाता है। यही चक्र साल-दर-साल चलता रहता है और किसान के लिए आत्महत्या के अलावा सभी दरवाजे एक-एक कर बंद होते जाते हैं।
दरअसल, कृषि-खाद्य तंत्र में फसल पैदा करना इस तंत्र का केवल एक हिस्सा है। इस तंत्र का सबसे लाजिमी हिस्सा होते हुए भी पूरे खाद्य तंत्र में इसका मूल्य योगदान मात्र 10 फीसदी है। 90 फीसदी हिस्से पर कृषि लागत तैयार करने वाली, भण्डारण और ढुलाई करने वाली, खाद्य प्रसंस्करण और खेती की उपजों को उपभोक्ता माल में बदलने वाली कंपनियों का कब्ज़ा है। आज खेती और किसान उर्वरक, कीटनाशक, डीजल जैसे लागतों को ब्रेड, बिस्कुट जैसे उपभोक्ता मालों में बदलने का जरिया भर है। किसान का न तो अपनी लागतों पर हक है और न ही अपनी उपज पर वह खेती तो करता है लेकिन खेती के बारे में कोई फैसला करने की हैसियत उसकी नहीं है। वह भले ही जमीन का मालिक हो लेकिन फसल तैयार करने से लेकर लोगों तक तैयार माल पहचाने की पूरी कड़ी में केवल एक मजदूर है।
कृषि खाद्य तंत्र पर काबिज कम्पनियों की चौतरफा लूट से जहां एक और कंपनियों के पास पूंजी का अम्बार जमा हुआ है वहीं दूसरी और किसानों की भारी आबादी का कंगालीकरण हुआ है, उनकी खरीददारी की ताकत तेज़ी से घटी है। कम्पनियों के पास जमा पूूंजी के अम्बार को फिर से कहीं लगाने के विकल्प लगातार घटते जा रहे हैं। किसानों समेत पूरी आबादी की खरीददारी की ताकत घटते जाने से कम्पनियों को उत्पादन घटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह संकट ऐसे मोड़ पर आकर फंस गया है यहां से इसके निकलने का एकमात्र रास्ता है किसानों की आमदनी का बढऩा, लेकिन इस रास्ते पर जाने की शर्त है लागतों और उपभोक्ता मालों पर कंपनियों की कब्जेदारी और मुनाफे की लूट की जगह किसानों और जनता के अधिकारों और जरूरतों को स्थापित करना। निश्चय ही ऐसी कोई भी तबदीली दुनिया के मौजूदा शासकों को मंजूर नहीं हैं।
मशीनी युग के आने से बनी नयी दुनिया में यह मुमकिन नहीं है कि खेती बिना किसी तबदीली के पुराने ढर्रे पर ही चलती रहे। लेकिन यह तय किया जा सकता है कि ये तब्दीलियां मुठ्ठी भर पूंजीपतियों के हक़ में हो या किसानों की भारी आबादी और तमाम जनता के हक़ में। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुके खेती के संकट के समाधान का जो रास्ता इन दोनों पुस्तकों में सुझाया गया है वह खेती के क्षेत्र में चीन के तजुर्बे से निकला है।
1949 में चीन में साम्राज्यवादी और सामंती ताकतों को हराकर किसानों और मजदूरों के मेल की सरकार सत्ता में आयी थी। इस नयी सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले क्रान्तिकारी भूमि सुधार के काम को हाथ में लिया। बड़े-बड़े समान्त जो जमीन कब्जाए बैठे थे उसे छीनकर किसानों के बीच बांट दिया। समान जोत वाले किसानों के सहकार कायम किये। इसने चीनी किसानों की बेडिय़ों को काट डाला और उनके सामने तरक्की का रास्ता खोल दिया। उन्होंने खेती का अंधाधुंध मशीनीकरण करने के बजाय शुरुआत में अपने किसानों के श्रम को ही खेती के विकास का आधार बनाया। अपने देश की खेती की हालत के मुताबिक खुद बीज, उर्वरक और मशीनें विकसित की। इस काम के लिए जरुरी कृषि विश्वविद्यालयों और शोध केन्द्रों को किसानों के नियंत्रण में देहातों में स्थापित किया। खेती से जुड़े छोटे उद्योगों को भी किसानों के साझे नियंत्रण में स्थापित किया। इससे किसानों की विशाल श्रमशक्ति के इस्तेमाल की दर बहुत ज्यादा बढ़ गयी जिससे उनकी साझी आमदनी में भारी बढ़ोत्तरी हुई।
जब खेती से आई यह बचत किसानों के पास इकठ्ठा हुई तो उन्होंने इसके एक छोटे हिस्से का इस्तेमाल अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में और दूसरे बड़े हिस्से का इस्तेमाल खेती के लिए नयी-नयी लागतें तैयार करने में किया। इससे किसानों की विशाल आबादी ग्राहक के रूप में तैयार हुई जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रफ़्तार को तेज कर दिया। खेती में नयी लागतों के इस्तेमाल ने पैदावार में भारी बढ़ोत्तरी की जिसके चलते दूसरे चक्र में किसानों की साझी आमदनी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आयी। किसानों ने ऐसे कई चक्रों की आमदनी को इकठ्ठा करके उपभोक्ता माल तैयार करने वाले उद्योग भी अपने साझे मालिकाने में लगाने शुरू किये। धीरे-धीरे हुए खेती के मशीनीकरण से किसान आबादी का जो हिस्सा मुक्त हुआ था उसे अपने खेतों के साथ ही जुड़े इन नये उद्योगों में काम मिलता गया।
चीन का बराबरी पर आधारित यह निजाम भारत, पकिस्तान जैसे देशों से बिलकुल अलग था। इन देशों में कभी भी मुकम्मल भूमि सुधार का काम ही नहीं हुआ और किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा भूमिहीन ही बना रहा। जिसके चलते बराबरी पर आधारित किसानों के सहकार भी कायम नही किये गये। शुरुआत से ही खेती को उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करने वाली और उनके तैयार माल को लागत के रूप में खपाने वाली चीज़ ही समझा गया। इसी का नतीजा है की आज इन देशों की भारी भूमिहीन आबादी कंगालीकरण का शिकार है और छोटी जोत वाली किसानों की भारी आबादी उद्योगों, बैंको और साहूकारों की लूट से पस्त होकर आत्महत्या की और बढऩे के लिए मजबूर हैं।
चीन की मेहनतकश जनता द्वारा शुरू किये गये महान प्रयोग की मंजिल एक ऐसा समाज बनाना था जहां देहात पर शहरों का, खेती पर उद्योग का और शारीरिक श्रम पर दिमागी श्रम का प्रभुत्व न हो। लेकिन 1980 के दशक में आयी देंग शियाओ पिंग की सरकार ने नयी उदारवादी नीतियों को अपनाकर चीनी जनता के इस महान प्रयोग की बालहत्या कर दी और चीन की खेती को भी उसी रस्ते पर धकेल दिया जहां किसान केवल कम्पनियों का कारिन्दा बन जाता है।
खेती के संकट के समाधान के लिए आज अलग-अलग लोग तरह-तरह के उपाय सुझाते हैं। कोई जैविक खेती की बात करता है तो कोई फिर से हल-बैल के जमाने में लौट जाने का रास्ता दिखाता है। कोई किसानों को कामचोर और नपुंसक ठहरता है तो कोई उन्हें ज्यादा पैदावार करने का दोषी बताता है। कोई सफ़ेद मूसली और जटरोफा की खेती करने की सलाह देता है। इसके विपरीत यह पुस्तक साबित करती है कि आज का खेती का संकट लूट पर टिकी पूंजीवादी व्यवस्था का संकट है। और इस व्यवस्था में इस संकट का कोई समाधान नहीं हैं। यह पुस्तक यह भी साबित करती है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था को ढहाकर इसकी जगह एक समतावादी और जनता के आपसी सहकार वाली व्यवस्था बनाकर ही इस संकट का सच्चा समाधान हो सकता है।
सम्पर्क- 9582908960